-
जन्म-ग्रहण - संवत् 1881 | सन् 1824
कर्शनजी त्रिवाड़ी के इसी टङ्कारा के जीवापुर मोहल्ले घर में संवत् १८८१ वा सन् १८२४ ई० में एक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। यही पुत्र पीछे घर छोड़कर निकल गये और संन्यासाश्रम ग्रहण करके संसार में स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए।
इससे पहले काठियावाड़ प्रदेश सिंहों के लिए ही प्रसिद्ध था। अब वह कर्शनजी के घर पुरुषसिंह को जन्म देकर गौरव के प्रोज्ज्वल मुकुट से मुकुटित हो गया। यह पुत्र कर्शनजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। नामकरण का समय आने पर कर्शनजी ने उनका नाम मूलजी रखा।
-
बाल-शिक्षा एवं विद्या आरम्भ - संवत् 1889 | सन् 1833
पाँच वर्ष की अवस्था में मूलजी का विद्यारम्भ हुआ। बाल्य-शिक्षा-विद्यारम्भ के तीन वर्ष बाद अर्थात् ८ वर्ष की अवस्था में मूलजी का उपनयन-संस्कार हुआ।
इसके अतिरिक्त कर्शनजी अपने पुत्र को अपने समान धर्मनिष्ठ और शिवभक्त बनाने के लिए उद्योग करने लगे। इसलिए उपनयन के दो वर्ष पश्चात् से ही अर्थात् दस वर्ष की अवस्था में उन्होंने बालक मूलजी को पार्थिव पूजा का आदेश और उपदेश दे दिया। इसके अतिरिक्त जब कभी कहीं किसी शिव-प्रसङ्ग की आलोचना वा शिव-माहात्म्य का कीर्तन होता तो मूलजा का अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता। -
मुर्त्तिपूजा में अविश्वास - संवत् 1894 | सन् 1838
जब मूलजी की अवस्था तेरह वर्ष की थी तो उनके पिता ने उन्हें शिवरात्रि का व्रत ग्रहण करने का आदेश किया। जड़ेश्वर के विशाल मन्दिर के भीतर जब मूलजी अकेले बैठे हुए जागरण कर रहे थे, मन्दिर की निस्तब्धता ने मन्दिर के चारों ओर की निस्तब्धता से मिलकर एक नयी निस्तब्धता की सृष्टि कर दी थी और शिव-चतुर्दशी के घोर तिमिरावरण में वह महानिस्तब्धता अविरत रहकर जिस समय मनुष्य के मन में आतंक का उद्दीपन कर रही थी, ऐसे समय में संशय के एक प्रबल झटके ने मूलजी के मन में प्रवेश करके उसे आलोडित कर डाला। इस विषय का उन्होंने स्वयं इस प्रकार वर्णन किया है-
“जब मैं मन्दिर में इस प्रकार अकेला जाग रहा था तो एक घटना उपस्थित हुई। कई चूहे बाहर निकलकर महादेव की पिण्डी के ऊपर दौड़ने लगे और बीच-बीच में महादेव पर जो चावल चढ़ाये गये थे, उन्हें भक्षण करने लगे। मैं जाग्रत् रहकर चूहों के इस कार्य को देखने लगा। देखते-देखते मेरे मन में आया कि यह क्या है ? जिस महादेव की शान्त, पवित्र मूर्ति की कथा, जिस महादेव के प्रचण्ड पाशुपतास्त्र की कथा और जिस महादेव के विशाल वृषारोहण की कथा गत दिवस व्रत के वृत्तान्त में सुनी थी, क्या वह महादेव वास्तव में यही है? इस प्रकार मैं चिन्ता से विचलित-चित्त हो उठा। मैंने सोचा कि यदि यथार्थ में यह वही प्रबल प्रतापी, दुर्दान्तदैत्यदलनकारी महादेव है तो यह अपने शरीर से इन थोड़े-से चूहों को क्यों विताड़ित नहीं कर सकता? इस प्रकार बहुत देर तक चिन्ता-स्रोत में पड़कर मेरा मस्तिष्क घूमने लगा। मैं आप ही अपने से पूछने लगा कि जो चलते-फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं डमरू बजाते हैं और मनुष्य को शाप दे सकते हैं, क्या यह वही वृषारूढ़ देवता हैं जो मेरे सामने उपस्थित हैं? यह प्रश्न वास्तव में सरल और स्वाभाविक है, परन्तु उसका उठाना तेरह वर्ष के बालक के लिए सम्भव मालूम नहीं होता, परन्तु जो भावी जीवन में महापुरुषों की पूज्य और उन्नत पदवी पर आरूढ़ होकर मनुष्यजाति की चिन्ता, सङ्कल्प और लक्ष्य को परिचालित करते हैं, उनका बाल्य-जीवन भी निःसन्देह किसी-न-किसी अंश में महापुरुष का परिचायक होता है। जर्मनी के प्रज्वलगौरव गेटे जब छह वर्ष के बालक थे तो उन्होंने लिस्बन के भीषण भूकम्प का समाचार सुनकर कहा था-"तो ईश्वर फिर दयालु कैसे हैं?" -
गृह-त्याग - संवत् 1903 | सन् 1846
मूलजी ने टङ्कारा में वापस आकर देखा कि विवाहोपयोगी सारा कार्य प्रायः प्रस्तुत हो गया है। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि माता-पिता उन्हें अब अधिक ज्ञानालोचना के कार्य में रत नहीं रहने देंगे और उनका विवाह किये बिना निश्चिन्त न होंगे। उस समय मूलजी ने इक्कीसवें वर्ष में प्रवेश किया था। जिस वैराग्यवह्नि ने तीन वर्ष पहले मूलजी के अन्तःकरण में केवल धूम्रमाला का विस्तार किया था अब वह धधक उठी और उनका निवृत्ति का सङ्कल्प अब दृढ़तर और प्रबलतर हो गया। उन्होंने स्थिर कर लिया कि मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिसके करने से मुझमें और मेरे विवाह में सदा के लिए प्रतिबन्धक हो जाए। ऐसा स्थिर करके उन्होंने एक दिन सन्ध्या समय संवत् १९०३ सन् १८४६ ई० में किसी से कुछ न कहकर सदा के लिए गृह-त्याग दिया । कर्शनजी का घर विवाहकार्यजनित आनन्द से परिपूर्ण हो रहा था, वह अब विषाद और शोक की समागमभूमि बन गया।
-
संन्यास प्रवेश - संवत् 1904 | सन् 1847
चाणोद, कर्णाली पहुँचने के बाद की घटना के विषय में शुद्धचैतन्य ने लिखा है-“वहाँ मैंने कई ब्रह्मचारियों, चिदानन्द प्रभृति संन्यासियों और कई योगदीक्षित साधुमहात्माओं के दर्शन किये। पहले योगदीक्षित साधओं को कभी नहीं देखा था, प्रथमत: कई दिन के शास्त्रालाप के पश्चात् मैं एक दिन परमानन्द परमहंस के पास गया और उनसे शिक्षा देने की प्रार्थना की। कुछ महीनों में ही मैंने वेदान्तसार और वेदान्त-परिभाषा के ग्रन्थों को पढ़ लिया।" चाणोद, कर्णाली की अवस्थिति के दिनों में शुद्धचैतन्य के मन में संन्यासाश्रम में प्रवेश करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। किन-किन कारणों से उनमें इन इच्छाओं का उदय हुआ, उनके विषय में वे लिखते हैं—“चूँकि मैं ब्रह्मचारी था, इस लिए मुझे ही अपने हाथ से भोजन पकाना पड़ता था। इससे अध्ययन में विघ्न होता था, विशेषकर इस कारण से भी कि मैंने उस समय तक अपना नाम नहीं त्यागा था। पितृकुल की प्रसिद्धि के कारण कोई बात करने में मुझे पहचान ले और जान ले कि अमुक कुल की सन्तान हूँ, इससे सदा भयभीत रहता था और अपना नाम बदलने के लिए भी चिन्तित रहता था। संन्यासाश्रम में प्रवेश करने से ये दोनों अड़चनें मिट जाएँगी, अत: मैं सन्यास दीक्षा करने के लिए उत्सक था।.....पूर्णानन्द इस पर सहमत हो गये और तीसरे दिन दीक्षित करके मुझे 'दयानन्द सरस्वती' नाम प्रदान कर दिया।
-
दण्डी विरजानन्द मिलन - संवत् 1917 | सन् 1860
मथुरा पहुँचकर पहले दयानन्द कुछ दिन रङ्गेश्वर के मन्दिर में ठहरे फिर एक दिन विरजानन्द की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया और अपना सङ्कल्प उनपर प्रकट किया। विरजानन्द जो अन्य विद्यार्थियों से कहा करते थे, वही उन्होंने दयानन्द से भी
कहा। विरजानन्द ने कहा-“आज तक जो कुछ तुमने मनुष्यप्रणीत ग्रन्थों में पढ़ा है, वह सब भूल जाओ, क्योंकि जब तक मनुष्यप्रणीत ग्रन्थों का प्रभाव रहेगा तब तक आर्षग्रन्थों का प्रकाश तुम्हारे चित्त में प्रवेश न कर सकेगा और यदि कोई मनुष्यप्रणीत ग्रन्थ तुम्हारे पास हो तो उसे यमुना के प्रवाह में फेंक आओ। एक और बात है, तुम संन्यासी हो, मैं कभी किसी संन्यासी को विद्यार्थीरूप से ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसके भोजन और रहने के स्थान की स्थिरता न हो वह मनोयोग के साथ विद्याभ्यास कैसे कर सकता है? इसलिए पहले तुम अपने खाने-पीने और रहने के स्थान की व्यवस्था कर आओ और फिर मेरे पास आकर विद्याभ्यास में लगो।" -
विद्या समाप्ति और गुरु दक्षिणा - संवत् 1920 | सन् 1863
इस देश में यह प्रथा चली आती है कि शिक्षा-समाप्ति पर शिष्य गुरु को दक्षिणा दिया करता है। अध्ययन-समाप्ति पर विद्यार्थीगण अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते हैं। शिष्यों से पढ़ाने की कोई दक्षिणा ग्रहण करना वा किसी अन्य प्रकार से अर्थ ग्रहण करना विरजानन्द के सङ्कल्प के विरुद्ध था। वे अपने शिष्यों से कोई दक्षिणा नहीं लिया करते थे। विशेषकर दयानन्द से तो वे क्या दक्षिणा लेते? वे तो संन्यासी थे, फूटी कौड़ी तक पास न थी, इनके पास दक्षिणा के लिए रुपया कहाँ से आता? जब दयानन्द गुरु विरजानन्द के पास विदा होने को गये तो गुरुदेव ने प्रेम के साथ कहा—'सौम्य! मैं तुमसे किसी प्रकार के धन की दक्षिणा नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे जीवन की दक्षिणा चाहता हूँ। तुम प्रतिज्ञा करो कि जितने दिन जीवित रहोगे उतने दिन आर्यावर्त में आर्षग्रन्थों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रन्थों का खण्डन करोगे और भारत में वैदिक धर्म की स्थापना में अपने प्राण तक अर्पण कर दोगे। दयानन्द ने इसके उत्तर में केवल एक शब्द कहा-"तथास्तु।" यह कहकर गुरुदेव के चरणों में प्रणत हो गये और फिर उन्होंने मथुरा से प्रस्थान कर दिया।
दयानन्द जीवन-दान करके संसार को जीवन प्रदान करने के लिए गुरुदेव से विदा हुए।
-
पाखण्ड खण्डिनी पताका (हरिद्वार) - संवत् 1924 | सन् 1867
संवत् १९२४ वि० सन् १८६७ ई० (७ मार्च-मई १८६७) हरिद्वार ( फाल्गुन शु० १ सं० २३ वैशाख सं० १९२४) खण्डन-पताका—हरिद्वार पहुँचकर स्वामीजी सप्तसरोवर पर ठहरे जो हृषीकेश और हरिद्वार के बीच में हरिद्वार से तीन कोस पर है। वहाँ बाड़ा बाँधकर और ८-१०छप्पर डालकर उन्होंने डेरा किया और एक पताका गाड़ दी, जिस पर 'पाखण्ड-खण्डन' शब्द लिखे हुए थे। उस समय १५१६ संन्यासी और ब्राह्मण उनके साथ थे, उनके वस्त्र गेरुआ थे, गले में रुद्राक्ष की माला थी, जिसमें एक स्फटिक का मनका पड़ा हुआ था।
-
आर्यसमाज की स्थापना - संवत् 1932 | सन् 1875
चैत्र शुक्ला ५ शनिवार संवत् १९३२ एवं १० अप्रैल १८७५ एवं (३ रवीउल अव्वल सन् १२९२ हिजरी, एवं शाके शालिवाहन १७९५, एवं फसली सन् १२८३, एवं खुर्दाद सन् १२८४ पारसी) को गिरगाम रोड में प्रार्थना-समाज के मन्दिर के निकट डॉक्टर माणकजी की बागबाड़ी में सायङ्काल के साढ़े ५ बजे एक सभा की गई जिसमें आर्यसमाज स्थापित किया गया।
-
चाँदपुर मेला - संवत् 1933 | सन् 1877
(१५ मार्च - २२ मार्च) चाँदापुर (चै० कृ ० ३०-चै० शु० ८ सं० ३४) शास्त्रार्थ चाँदापुर – इस मेले का नाम ' मेला ब्रह्म-विचार' रखा गया था और १९ मार्च से २३ मार्च तक उसका समय नियत किया गया था । मेला-भूमि में डेरे तम्बू आदि लगा दिये गये थे। आगन्तुकों के सुभीते के लिए खाद्य पदार्थों की दुकानों आदि का भी प्रबन्ध था । मेला संस्थापकों ने मेले के विज्ञापन नगर-नगर में भेजवा दिये थे और आर्यधर्म, ईसाई और मुसलमानी मत के मुख्य उपदेशकों को भी निमन्त्रित किया था तथा उनके ठहरने, आहार- पानादि का भी हर एक प्रकार से सुप्रबन्ध कर दिया था।
-
निर्वाण दिवस - संवत् 1940 | सन् 1883
चार बजे के समय बाहर से आये हुए आर्यपुरुष महाराज के समीप गये और सामने खड़े हो गये। महाराज ने सबको ऐसी कृपादृष्टि से देखा कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, मानो वे सबसे यह कह रहे थे कि उदास क्यों होते हो, सबको धैर्य धारण करना चाहिए ।
उस समय महाराज के मुख पर किसी प्रकार के शोक व घबराहट के चिह्न न थे। अपने घोरतम कष्ट को इस प्रकार सहन करते थे कि मुख से एक बार भी 'हाय' या अन्य कष्टसूचक शब्द न निकलता था । महाराज बड़ी सावधानी से रहे और बातचीत करते रहे ।
इतने में पाँच बज गये। महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप श्रीमानों का चित्त कैसा है तो कहा अच्छा है, तेज और अन्धकार का भाव है । इस बात को लोग कुछ न समझे ।
जब साढ़े पाँच बजे तो महाराज ने कहा कि जो लोग हमारे साथ हैं तथा दूरस्थ स्थानों से आये हैं उन्हें बुलाकर हमारे पीछे खड़ा कर दो, सामने कोई खड़ा न हो । जब सब लोग आ गये तो महाराज ने कहा कि चारों ओर के द्वार खोल दो और छत के दो रोशनदान भी खुलवा दिये और पूछा कि कौन-सा पक्ष, क्या तिथि और क्या वार है ? किसी ने उत्तर दिया कि कृष्णपक्ष का अन्त और शुक्ल का आदि अमावस्या और मंगलवार है । यह सुनकर छत और दीवारों की ओर दृष्टि की, फिर कई वेदमन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् संस्कृत में ईश्वरोपासना की और भाषा में ईश्वर का गुण-कीर्त्तन किया और फिर बड़ी प्रसन्नता और हर्षपूर्वक गायत्रीमन्त्र का पाठ करने लगे और कुछ देर तक समाधिस्थ रहकर आँखें खोल दीं और यों कहने लगे
'हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमन् ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है तेरी इच्छा पूर्ण हो, आहा !!! तैंने अच्छी लीला की ।' महाराज उस समय सीधे लेट रहे थे, ये शब्द कहकर उन्होंने स्वयं करवट ली और एक प्रकार से श्वास को रोककर एकदम बाहर निकाल दिया। महाराज की मानवी लीला समाप्त हुई और उनका आत्मा नश्वर देह को छोड़कर जगज्जननी की प्रेममयी गोद में जा विराजा । महाराज के शरीर छूटने के समय छह बजे थे।
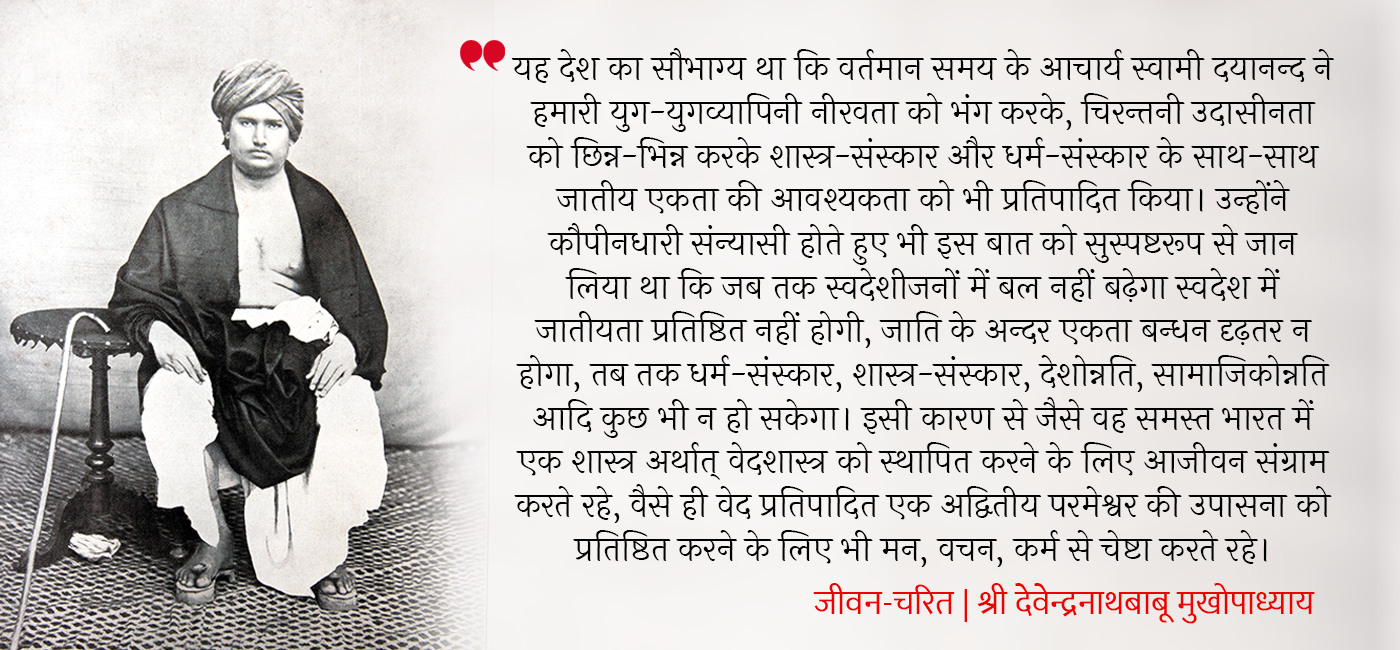

 English
English